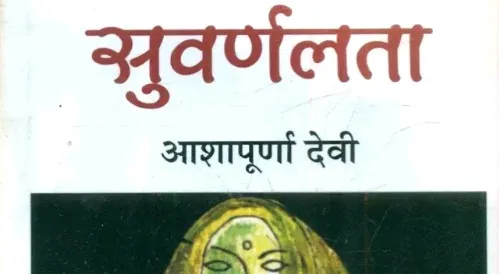सुवर्णलता/आशापूर्णा देवी
"प्रथम प्रतिश्रुति" के बाद "सुवर्णलता" पढ़ रही हूँ और चाहे सत्यवती की कथा रही हो या सुवर्ण की, उपन्यास पढ़ते हुए बार-बार ध्यान बीच में अपने अतीत की उन काली छायाओं की ओर जा पहुँचता है जिसका उपन्यास की कथा से सुमेल दिखलाई पड़ता है। एक खुली खिड़की, एक टुकड़ा आसमान, एक आत्मीय और समझने जाने वाले मन की चाहना में भटकती छिप-छिप कर पुस्तकें पढ़ती, विकट बंधनों से बंधी फिर भी से बंधनमुक्त और कलुष रहित सुवर्ण को पढ़ते हुए उसमें क्या अपनी परछाई नहीं दिखलाई पड़ती या अपने आसपास के असंख्य स्त्रियों की झलक । सत्यवती की हो सुवर्ण की या बकुल की तीन कालखंडो में बंटी वह कथा तो बहुत पहले की है मगर क्या स्त्रियों का जीवन किसी न किसी तौर पर अब भी ठीक वैसा नहीं है । कितना कुछ बदला है फिर भी कितना कुछ जस का तस है । दशा बदली और दिशा बदली फिर भी बहुत कहाँ बदली है ? उस तरह कहाँ बदली जिस तरह बदलनी चाहिए थी । पुरूष का मानस स्त्री के प्रति सभ्य ही कहाँ हो पाया अब तक ? कहाँ देख पाया वह उसे मनुष्य की दृष्टि से ?
बहुत पीछे क्यों जाऊँ कल उपन्यास पढ़ते हुए मन में सहजा वह दिन बिजली की तरह कौंध उठा । सात-आठ बरस पहले की वह बात । गलियारे में हो हुल्लड़ मचा था । मैं बरतन माँजना छोड़ द्वार पर पहुँची तो देखती हूँ दूसरे मुहल्ले के बच्चे हमारे घर के बिल्ली के नन्हे बच्चे को उठाये लिए जा रहे हैं मैंने गली में उतरकर उन्हें डाँट लगाई और बच्चा छुड़ा लिया । इतने में मेरा भाई आवाज़ सुनकर घर से बाहर निकला और मेरी बाँह पकड़कर भीतर की ओर ठेलते हुए बोला - चलो भीतर चलो। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो ? उन दिनों वह किशोर उम्र का ही था मगर फिर भी उसके लिए मेरा दरवाजे पर खड़ा होना शर्म और अपमान का कारण बन गया ।
मैंने जो कहा और किया था वह कोई अनुचित और आपत्ति जतलाने योग्य बात नहीं थी मगर बाद उसके वह जो मेरी बाँह पकड़ भीतर ले आया, वह इतनी पीड़ादायक और गलत बात थी कि मेरे अंतर में काँटे सी चुभ गई। उसने जिस तरह मुझे भीतर की ओर ठेला उस दुख और अपमान से गला अवरुद्ध हो गया था। बेड़ियों और जंजीरों में जकड़े होने के साथ-साथ गूँगे होने जैसा अनुभव हुआ । भाई को तो क्या याद होगी उस दिन की अब लेकिन मैं तो स्त्री हूँ और स्त्री कभी कुछ नहीं भूलती। आज वही भाई है जो एक रोज मुझे घर के दरवाजे पर आते-जाते लोंगो के बीच खड़े और बोलते देख शर्म से गढ़ गया था वही आज कहीं जाना होता है तो मुझे स्टेशन छोड़ आता है। एक बार भी उसके मन में यह नहीं आता कि अकेले जा रही है और अकेले जाना सही नहीं है। मगर ऐसा नहीं है कि उम्र बढ़ने के साथ-साथ अपने आप उसमें हृदय परिवर्तन हो गया । वह चीजें मैंने बदली हैं प्रयास करके, जतन से, मेहनत से रास्ता बनाने के लिए प्रयास जरूर किया है सिर्फ़ अपने लिए नहीं अपने बाद की स्त्रियों के लिए । अपने घर की उन लड़कियों, बच्चियों और स्त्रियों के लिए जो अभी इस संसार में भी नहीं आई हैं। बनाने में सफल कितना हो पाई हूँ या आगे कितना हो पाऊँगी वह नहीं जानती । मगर यह जानती हूँ हमें इसी तरह सोचने विचारने और आगे बढ़ने की आवश्यकता है।
ऊपर जो बात कही अपने से जुड़ी जो घटना उठाई वह बात बहुत छोटी सी है मगर औरतों का जीवन तो इतना अभावों भरा रहा होता है कि अगर उनके पास चेतना है और वे संवेदनशील हैं तो उसके लिए हर छोटी चीज बड़ी हो जाती है। मेरे जीवन में इस तरह घटे किस्से और भी हैं असंख्य हैं मगर वे फिर कभी सही। मगर मैं बीते कई सालों कई सालों से लगातार इस पर सोचती विचारती रही हूँ कि स्त्रियाँ अपने बच्चों खासकर पुरुष संतानों को बड़ा करते समय इस जड़ता से इस मानसिकता संक्रीर्णता से मुक्त करने का प्रयास क्यों नहीं करती? अब भी नहीं करती जबकि दुनिया कितनी बदल गई है। फिर आप से ही उत्तर भी पा लेती हूँ कि खुद भी कहाँ बदल पाई है इतनी अधिक संख्या में जो वे अपनी आधी आबादी को उस ओछे और छोटेपन से मुक्त करने के लिए प्रयासरत हों। और दूसरे को तो वही प्रभावित सकता है बेहतर का संकल्प तो वही भर सकता है जिसकी अपनी मानसिक अवस्था बेहतर की ओर अग्रसर हुई हो ।कितनी स्त्रियों की हुई है कितनी बैठकर इस तरह सोचती विचारती हैं इस पर विचारों तो परिणाम बहुत भले और बेहतर नहीं दिखलाई पड़ते।
"प्रथम प्रतिश्रुति" और "सुवर्णलता" पढ़ते हुए मुझे यह भी महसूस होता रहा जो इसमें दर्ज हैं वैसे विकट बंधनों, पीड़ाओं, अभावों, अन्याय, अपमान और अत्याचार झेलती सहती इन सबसे घिरी महिलाएँ महिलाएँ तो मैंने अनेक देखीं, सबकी लगभग कम अधिक एक सी कहानी रही हैं। फिर भी अपने जीवन में मुझे वैसी वास्तव में देखी हुई एक भी स्त्री नहीं याद आती जिसमें ऐसी चेतना या इसकी कौंध भी मैंने कभी देखी हो जो इन नायिकाओं में रही है । जबकि ऐसा तो नहीं है कि ऐसी स्त्रियाँ सिर्फ़ उपन्यासों की पात्र रही होंगी । वास्तव में वे हुई ही न हों ऐसा भी नहीं है मगर वे इतनी कम हुई हैं कि ढूँढने पर ही मिलती है । और जब मिलती हैं तो यहाँ की नहीं किसी और दुनिया की जान पड़ती हैं । आशापूर्णा देवी ने ऐसी नायिकाओं को उपन्यासों का पात्र बनाया ही संभवतः इसीलिए है कि हैं नहीं तो इस तरह की स्त्रियाँ होनी चाहिए । संघर्षो से भरा रहे उनका जीवन मगर बनी रहे, बची रहे हर युग में पैदा होती रहें ।
"सुवर्णलता" में ही एक जगह आशापूर्णा देवी जो यह एक लिखती हैं वह भी पढ़ने और मनन करने योग्य हैं -
ईर्ष्यापरायण पुरूष समाज कब मुक्त हृदय से कह पायेगा, " हम तुम्हें जो स्वीकृति नहीं दे पाये हैं, वह तुम्हारी त्रुटि का नतीजा नहीं है, वह हमारी त्रुटि का परिणाम है ! तुम्हारी महिमा को मर्यादा देने में जो झिझक होती है, वह हमारी दुर्बलता है, तुम्हारी शक्ति को प्रणाम जो नहीं कर पाते हैं, वह हमारा दैन्य है। अपने को तुम्हारा 'प्रभु' कहने की आदत छोड़ने में हमारे अभिमान को आँच आती है। इसलिए दास बनकर तुम्हें 'रानी' बनाते हैं। आज भी तुम्हें मुग्ध करके अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं; इसीलिए चाटुकारिता से तुम्हें भुलाते हैं और अपने शिल्प-साहित्य-काव्य में तुम्हारी वेदना के जो गीत गाते हैं, वह केवल अपने को विकसित करने के लिए ! तुम हमारे प्रदीप से आलोकित हो, हमारी साध यह है; अपनी महिमा से तुम भास्वर हो, इसमें हमे आपत्ति है। इसलिए जब तुम अपने गुण का परिचय देती हो, तो करूणा की हँसी हँसकर पीठ थपथपाते हैं, जब शक्ति का परिचय देती हो, तो खीझ की भृकुटी करके कहते हैं, यह ढिटाई है और जब बुद्धि का परिचय देती हो, तब तुम्हें हेय करने के लिए पीछे पड़ जाते हैं !
तुम्हारी रुपमती मूर्ति के हम मुग्ध भक्त हैं, तुम्हारी भोगमती मूर्ति के हम आज्ञाकारी, सेवामयी मूर्ति के आगे बिके हुए और मातृमूर्ति के आगे हम शिशु मातृ हैं। लेकिन यह सारा कुछ एकांत भाव से हमारे लिए ही होना चाहिए। हाँ, जो तुम हमें अवलम्वन करके हो, केवल उसी 'तुम' को हम बर्दाश्त कर सकते हैं। उसके बाहर की 'तुम' विधाता की एक हास्यकर सृष्टि हो।"
- वियोगिनी ठाकुर
© All Rights Reserved
बहुत पीछे क्यों जाऊँ कल उपन्यास पढ़ते हुए मन में सहजा वह दिन बिजली की तरह कौंध उठा । सात-आठ बरस पहले की वह बात । गलियारे में हो हुल्लड़ मचा था । मैं बरतन माँजना छोड़ द्वार पर पहुँची तो देखती हूँ दूसरे मुहल्ले के बच्चे हमारे घर के बिल्ली के नन्हे बच्चे को उठाये लिए जा रहे हैं मैंने गली में उतरकर उन्हें डाँट लगाई और बच्चा छुड़ा लिया । इतने में मेरा भाई आवाज़ सुनकर घर से बाहर निकला और मेरी बाँह पकड़कर भीतर की ओर ठेलते हुए बोला - चलो भीतर चलो। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो ? उन दिनों वह किशोर उम्र का ही था मगर फिर भी उसके लिए मेरा दरवाजे पर खड़ा होना शर्म और अपमान का कारण बन गया ।
मैंने जो कहा और किया था वह कोई अनुचित और आपत्ति जतलाने योग्य बात नहीं थी मगर बाद उसके वह जो मेरी बाँह पकड़ भीतर ले आया, वह इतनी पीड़ादायक और गलत बात थी कि मेरे अंतर में काँटे सी चुभ गई। उसने जिस तरह मुझे भीतर की ओर ठेला उस दुख और अपमान से गला अवरुद्ध हो गया था। बेड़ियों और जंजीरों में जकड़े होने के साथ-साथ गूँगे होने जैसा अनुभव हुआ । भाई को तो क्या याद होगी उस दिन की अब लेकिन मैं तो स्त्री हूँ और स्त्री कभी कुछ नहीं भूलती। आज वही भाई है जो एक रोज मुझे घर के दरवाजे पर आते-जाते लोंगो के बीच खड़े और बोलते देख शर्म से गढ़ गया था वही आज कहीं जाना होता है तो मुझे स्टेशन छोड़ आता है। एक बार भी उसके मन में यह नहीं आता कि अकेले जा रही है और अकेले जाना सही नहीं है। मगर ऐसा नहीं है कि उम्र बढ़ने के साथ-साथ अपने आप उसमें हृदय परिवर्तन हो गया । वह चीजें मैंने बदली हैं प्रयास करके, जतन से, मेहनत से रास्ता बनाने के लिए प्रयास जरूर किया है सिर्फ़ अपने लिए नहीं अपने बाद की स्त्रियों के लिए । अपने घर की उन लड़कियों, बच्चियों और स्त्रियों के लिए जो अभी इस संसार में भी नहीं आई हैं। बनाने में सफल कितना हो पाई हूँ या आगे कितना हो पाऊँगी वह नहीं जानती । मगर यह जानती हूँ हमें इसी तरह सोचने विचारने और आगे बढ़ने की आवश्यकता है।
ऊपर जो बात कही अपने से जुड़ी जो घटना उठाई वह बात बहुत छोटी सी है मगर औरतों का जीवन तो इतना अभावों भरा रहा होता है कि अगर उनके पास चेतना है और वे संवेदनशील हैं तो उसके लिए हर छोटी चीज बड़ी हो जाती है। मेरे जीवन में इस तरह घटे किस्से और भी हैं असंख्य हैं मगर वे फिर कभी सही। मगर मैं बीते कई सालों कई सालों से लगातार इस पर सोचती विचारती रही हूँ कि स्त्रियाँ अपने बच्चों खासकर पुरुष संतानों को बड़ा करते समय इस जड़ता से इस मानसिकता संक्रीर्णता से मुक्त करने का प्रयास क्यों नहीं करती? अब भी नहीं करती जबकि दुनिया कितनी बदल गई है। फिर आप से ही उत्तर भी पा लेती हूँ कि खुद भी कहाँ बदल पाई है इतनी अधिक संख्या में जो वे अपनी आधी आबादी को उस ओछे और छोटेपन से मुक्त करने के लिए प्रयासरत हों। और दूसरे को तो वही प्रभावित सकता है बेहतर का संकल्प तो वही भर सकता है जिसकी अपनी मानसिक अवस्था बेहतर की ओर अग्रसर हुई हो ।कितनी स्त्रियों की हुई है कितनी बैठकर इस तरह सोचती विचारती हैं इस पर विचारों तो परिणाम बहुत भले और बेहतर नहीं दिखलाई पड़ते।
"प्रथम प्रतिश्रुति" और "सुवर्णलता" पढ़ते हुए मुझे यह भी महसूस होता रहा जो इसमें दर्ज हैं वैसे विकट बंधनों, पीड़ाओं, अभावों, अन्याय, अपमान और अत्याचार झेलती सहती इन सबसे घिरी महिलाएँ महिलाएँ तो मैंने अनेक देखीं, सबकी लगभग कम अधिक एक सी कहानी रही हैं। फिर भी अपने जीवन में मुझे वैसी वास्तव में देखी हुई एक भी स्त्री नहीं याद आती जिसमें ऐसी चेतना या इसकी कौंध भी मैंने कभी देखी हो जो इन नायिकाओं में रही है । जबकि ऐसा तो नहीं है कि ऐसी स्त्रियाँ सिर्फ़ उपन्यासों की पात्र रही होंगी । वास्तव में वे हुई ही न हों ऐसा भी नहीं है मगर वे इतनी कम हुई हैं कि ढूँढने पर ही मिलती है । और जब मिलती हैं तो यहाँ की नहीं किसी और दुनिया की जान पड़ती हैं । आशापूर्णा देवी ने ऐसी नायिकाओं को उपन्यासों का पात्र बनाया ही संभवतः इसीलिए है कि हैं नहीं तो इस तरह की स्त्रियाँ होनी चाहिए । संघर्षो से भरा रहे उनका जीवन मगर बनी रहे, बची रहे हर युग में पैदा होती रहें ।
"सुवर्णलता" में ही एक जगह आशापूर्णा देवी जो यह एक लिखती हैं वह भी पढ़ने और मनन करने योग्य हैं -
ईर्ष्यापरायण पुरूष समाज कब मुक्त हृदय से कह पायेगा, " हम तुम्हें जो स्वीकृति नहीं दे पाये हैं, वह तुम्हारी त्रुटि का नतीजा नहीं है, वह हमारी त्रुटि का परिणाम है ! तुम्हारी महिमा को मर्यादा देने में जो झिझक होती है, वह हमारी दुर्बलता है, तुम्हारी शक्ति को प्रणाम जो नहीं कर पाते हैं, वह हमारा दैन्य है। अपने को तुम्हारा 'प्रभु' कहने की आदत छोड़ने में हमारे अभिमान को आँच आती है। इसलिए दास बनकर तुम्हें 'रानी' बनाते हैं। आज भी तुम्हें मुग्ध करके अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं; इसीलिए चाटुकारिता से तुम्हें भुलाते हैं और अपने शिल्प-साहित्य-काव्य में तुम्हारी वेदना के जो गीत गाते हैं, वह केवल अपने को विकसित करने के लिए ! तुम हमारे प्रदीप से आलोकित हो, हमारी साध यह है; अपनी महिमा से तुम भास्वर हो, इसमें हमे आपत्ति है। इसलिए जब तुम अपने गुण का परिचय देती हो, तो करूणा की हँसी हँसकर पीठ थपथपाते हैं, जब शक्ति का परिचय देती हो, तो खीझ की भृकुटी करके कहते हैं, यह ढिटाई है और जब बुद्धि का परिचय देती हो, तब तुम्हें हेय करने के लिए पीछे पड़ जाते हैं !
तुम्हारी रुपमती मूर्ति के हम मुग्ध भक्त हैं, तुम्हारी भोगमती मूर्ति के हम आज्ञाकारी, सेवामयी मूर्ति के आगे बिके हुए और मातृमूर्ति के आगे हम शिशु मातृ हैं। लेकिन यह सारा कुछ एकांत भाव से हमारे लिए ही होना चाहिए। हाँ, जो तुम हमें अवलम्वन करके हो, केवल उसी 'तुम' को हम बर्दाश्त कर सकते हैं। उसके बाहर की 'तुम' विधाता की एक हास्यकर सृष्टि हो।"
- वियोगिनी ठाकुर
© All Rights Reserved